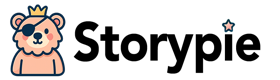टेलीविज़न का सपना
मेरा नाम फिलो फार्न्सवर्थ है, और मेरी कहानी एक ऐसी दुनिया में शुरू होती है जहाँ विचार हवा में तैरते थे, लेकिन तस्वीरें नहीं. मैं इडाहो के एक खेत में पला-बढ़ा, जहाँ दिन मेहनत और रातें सपनों से भरी होती थीं. मैं उस समय के नए आविष्कारों, जैसे टेलीफ़ोन और रेडियो से बहुत प्रभावित था. मैं घंटों बैठकर सोचता था कि कैसे एक अदृश्य शक्ति आवाज़ों को मीलों दूर तक ले जाती है. मेरे युवा मन में एक बड़ा सवाल घूमता रहता था: अगर हम हवा के ज़रिए आवाज़ भेज सकते हैं, तो तस्वीरें क्यों नहीं? यह सवाल मेरे साथ तब भी रहता, जब मैं अपने परिवार के खेत में काम करता. फिर 1921 की एक साधारण दोपहर में, जब मैं चौदह साल का था और आलू के खेत में हल चला रहा था, जवाब बिजली की तरह मेरे दिमाग़ में कौंध गया. मैंने हल को खेत में सीधी, समानांतर कतारें बनाते हुए देखा. अचानक मुझे एहसास हुआ! एक तस्वीर को भी ठीक इसी तरह, एक-एक करके कतारों में तोड़ा जा सकता है. एक इलेक्ट्रॉन की किरण का उपयोग करके, एक छवि को स्कैन किया जा सकता है, उसे बिजली में बदला जा सकता है, और फिर कहीं और फिर से जोड़ा जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे मैं ज़मीन की कतारें बना रहा था. उस दिन, एक आलू के खेत में, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न का विचार पैदा हुआ था.
खेत में आया वह सपना मेरे दिमाग़ पर छा गया. अब चुनौती यह थी कि इस सपने को एक काग़ज़ के टुकड़े से निकालकर असल दुनिया में लाया जाए. यह आसान नहीं था. मैंने अपना घर छोड़ा और कैलिफ़ोर्निया चला गया, जहाँ मैंने निवेशकों को अपने इस जंगली विचार के लिए पैसे देने के लिए मनाने की कोशिश की. कल्पना कीजिए, लोगों को यह समझाना कि मैं एक ख़ास तरह के काँच के जार में रोशनी को पकड़कर उसे बिजली में बदल सकता हूँ. कई लोगों ने सोचा कि मैं पागल हूँ, लेकिन कुछ ने मुझ पर विश्वास किया. उन पैसों से, मैंने एक छोटी सी प्रयोगशाला बनाई और अपनी टीम के साथ काम करना शुरू कर दिया. मेरे आविष्कार का दिल था 'इमेज डिसेक्टर' ट्यूब. यह एक वैक्यूम ट्यूब थी जिसे मैंने प्रकाश को पकड़ने और उसे इलेक्ट्रॉनों की एक धारा में बदलने के लिए डिज़ाइन किया था. हमने अनगिनत घंटे काम किया, कई बार असफल हुए, और हर असफलता से कुछ नया सीखा. यह एक पहेली को सुलझाने जैसा था, जहाँ हर टुकड़ा एक नई चुनौती पेश करता था. फिर, 7 सितंबर, 1927 को वह ऐतिहासिक दिन आया. हम सब अपनी साँस रोके हुए थे. मैंने ट्रांसमीटर चालू किया, और रिसीवर पर... एक सीधी, स्पष्ट क्षैतिज रेखा दिखाई दी. यह सिर्फ़ एक लकीर थी, लेकिन हमारे लिए यह पूरी दुनिया थी. हमने यह साबित कर दिया था कि हवा के ज़रिए तस्वीर भेजना संभव था. उस छोटी सी प्रयोगशाला में ख़ुशी की लहर दौड़ गई.
वह एक अकेली रेखा तो बस शुरुआत थी. हम जानते थे कि अगर हम एक रेखा भेज सकते हैं, तो हम और भी जटिल छवियाँ भेज सकते हैं. हमारा अगला लक्ष्य एक इंसान का चेहरा प्रसारित करना था. इस ऐतिहासिक क्षण के लिए, मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो मुझ पर भरोसा करे. 1929 में, मैंने अपनी प्यारी पत्नी, पेम से पूछा, “क्या तुम टेलीविज़न पर आने वाली पहली इंसान बनोगी?” वह मुस्कुराई और मान गई. उसने कैमरे के सामने बैठकर अपनी आँखें झपकाईं, और दूसरे कमरे में, रिसीवर की नीली-हरी स्क्रीन पर, उसकी धुँधली लेकिन पहचानने योग्य छवि दिखाई दी. यह एक जादुई क्षण था; हमने न केवल एक तस्वीर, बल्कि एक जीवित, साँस लेते इंसान की छवि को प्रसारित किया था. इस सफलता ने हमें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया. 1934 में, हमें फ़िलाडेल्फ़िया के फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट में अपने पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न सिस्टम को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का मौका मिला. लोग हैरान थे. उन्होंने इसे एक 'जादू का बक्सा' कहा जो चलती-फिरती तस्वीरों को हवा के माध्यम से खींच सकता था. उस दिन, मेरा आविष्कार सिर्फ़ एक प्रयोगशाला का प्रयोग नहीं रहा; यह एक ऐसी हक़ीक़त बन गया जिसे दुनिया देख और समझ सकती थी.
टेलीविज़न का आविष्कार करना एक बात थी, लेकिन यह साबित करना कि यह मेरा आविष्कार था, एक और बड़ी लड़ाई थी. मुझे अपने पेटेंट के अधिकारों के लिए बड़ी कंपनियों से मुक़दमा लड़ना पड़ा. यह एक थका देने वाली प्रक्रिया थी, लेकिन मैं जानता था कि मुझे अपने सपने के लिए खड़ा होना होगा. आख़िरकार, मेरे हाई स्कूल के शिक्षक की गवाही की मदद से, मैंने साबित कर दिया कि यह विचार मेरा ही था. लेकिन मेरी असली जीत अदालतों में नहीं, बल्कि दुनिया भर के घरों में हुई. जैसे-जैसे टेलीविज़न लोकप्रिय होता गया, यह परिवारों के लिए एक साथ आने का एक ज़रिया बन गया. यह दुनिया के लिए एक खिड़की बन गया. लोग अपने बैठक में बैठकर ख़बरें, मनोरंजन और ऐतिहासिक घटनाएँ देख सकते थे. मैंने कल्पना की कि कैसे परिवारों ने एक साथ बैठकर नील आर्मस्ट्रांग को चाँद पर पहला क़दम रखते हुए देखा होगा. मेरा छोटा सा आविष्कार, जो एक आलू के खेत में शुरू हुआ था, लोगों को इस तरह से जोड़ रहा था जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी. यह सिर्फ़ तस्वीरें भेजने के बारे में नहीं था; यह अनुभव और कहानियाँ साझा करने के बारे में था, जिसने दुनिया को थोड़ा छोटा और थोड़ा ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस कराया.
आज, जब मैं आपके स्मार्ट टीवी, लैपटॉप और फ़ोन को देखता हूँ, तो मुझे वही पुरानी जिज्ञासा दिखाई देती है. तकनीक बहुत बदल गई है, लेकिन मूल विचार वही है: कहानियों और छवियों को दूरियों के पार साझा करना. मेरा सपना एक आलू के खेत में एक साधारण सवाल से शुरू हुआ था. इसने मुझे सिखाया कि कोई भी विचार बहुत बड़ा या बहुत असंभव नहीं होता, अगर आपके पास उसे पूरा करने का जुनून और दृढ़ संकल्प हो. आपकी दुनिया संभावनाओं से भरी है. हो सकता है कि आपका अगला महान विचार आपके स्कूल की कक्षा में, खेल के मैदान में, या शायद अपने ही घर के आँगन में इंतज़ार कर रहा हो. इसलिए, हमेशा सवाल पूछते रहो. जिज्ञासु बनो. और सबसे महत्वपूर्ण, अपने सपनों का पीछा करने की हिम्मत रखो, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों न हों. कौन जानता है? शायद आप ही अगला आविष्कार करेंगे जो दुनिया को बदल देगा.
पढ़ाई की समझ के प्रश्न
उत्तर देखने के लिए क्लिक करें